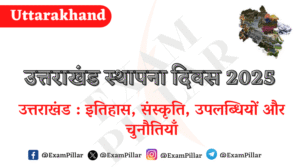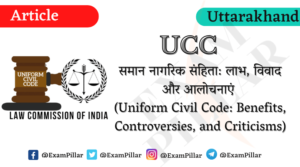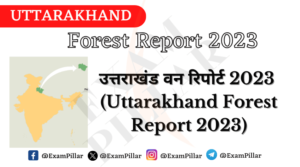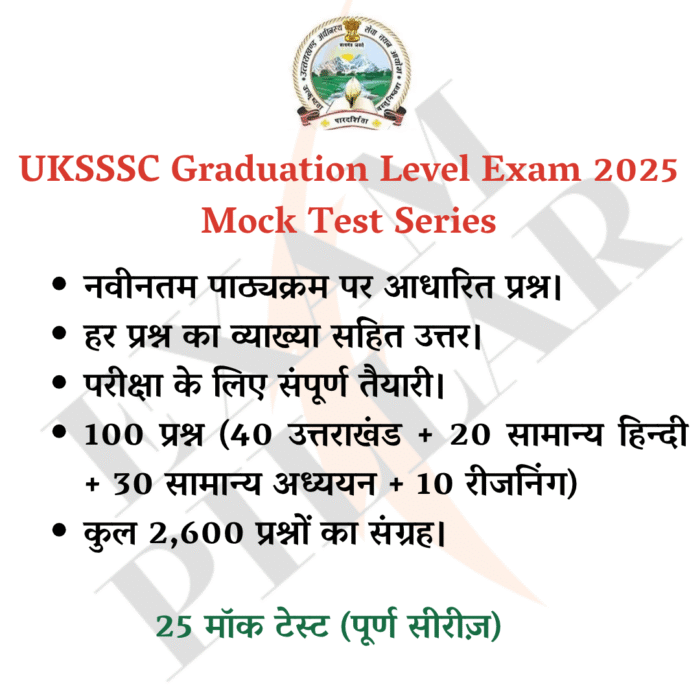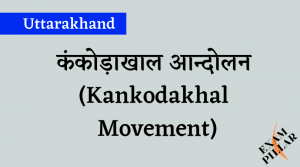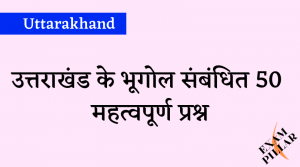अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा में मिट्टी कटान सबसे ज्यादा था। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सालों से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो मिट्टी कटान की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। 2017 में तैयार किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 24295 वर्ग किलोमीटर जंगल का क्षेत्र है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 45.43 फीसद है। उत्तराखंड की भूमि संरचना को देखते हुए, भूमि को तीन भागों में बांटा गया है। जो निम्न प्रकार से है –
उत्तराखंड में पायी जाने वाली मिट्टी
1. तालाब / नदी घाटी की भूमि
- उत्तराखंड में नदियां अपने प्रवाह मार्ग के सहारे विशाल उर्वरक मैदानों का निर्माण करती है।
- इन मैदानों में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होती है। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहां पर गेहूं, धान की खेती की जाती है।
- यह मध्यम कृषि क्षेत्र वाला प्रदेश है। और उत्तराखंड में सिंचित भूमि कोतलाव कहा जाता है।
2. मैदानी भागों की भूमि
- इसमें संपूर्ण तराई भाबर क्षेत्र आता है। जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल का कुछ भाग आता है।
- यहां पर समतल एवं उर्वरक मैदान है। तथा इन मैदानों में कृषि सर्वाधिक विकसित अवस्था में मिलती है।
- इन क्षेत्रों मेंगेहूं, धान, गन्ना एवं दलहनी फसलों का उत्पादन अधिक होता है।
3. पर्वतीय ढाल युक्त भूमि / उखड
- उत्तराखंड में पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती होती है।
- सिंचित भूमि ना होने के कारण स्थानीय भाषा में इसे उखड़ कहा जाता है। यह कृषि वर्षा पर आधारित होती है।
- जिस कारण उत्पादन कम तथा अनियंत्रित होता है। इसलिए वर्तमान में लोग कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य व्यवसायों में संलग्न हो गए हैं।
- ICAR (दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने उत्तराखंड की मिट्टी को पर्वतीय या वनीय मिट्टी कहा है।
मिट्टी के संगठन के आधार पर उत्तराखंड में निम्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं –
1. तराई मिट्टी
- राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से ऊधम सिंह नगर तक महिन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मृदा पाई जाती हैं।
- राज्य की अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा है।
- यह मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है।
- इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है।
2. भाबर मिट्टी
- भाबर मृदा तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण यह मृदा पाई जाती है।
- हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी कंकड़ों-पत्थरों तथा मोटे बालुओं से निर्मित है।
- यहां पर मिट्टी पथरीली एवं कंकड़ पत्थर से युक्त होती है, जिस कारण जल नीचे चला जाता है।
- यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है।
- पानी की कमी के कारण यह अनउपजाऊ होती है।
3. चारगाही मिट्टी
- ऐसी मृदाएं निचले भागों में जलधाराओं के निकट नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है।
- इस मृदा को निम्न पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है –
- मटियार दोमट (भूरा रंग, नाईट्रोजन तथा जैव पदार्थ अधिक एवं चूना कम)
- अत्यधिक चूनेदार दोमट
- कम चूनेदार दोमट
- गैर चूनेदार दोमट
- बलुई दोमट
4. टर्शियरी मिट्टी
- ये मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पायी जाती है जोकि हल्की, बलुई एवं छिद्रमय अर्थात् आद्रता को कम धारण करती है।
- इसमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है। लेकिन दून घाटी के मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति के अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है।
- ये शिवालिक एवं दून घाटी में पाई जाती है।
5. क्वाटर्ज मिट्टी
- यह मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पायी जाती है।
- आद्य, पुरा एवं मध्य कल्प के क्रिटेशियस युग में निर्मित शिष्ट, शेल, क्वार्ट्ज आदि चट्टानो के विदीर्ण होने से इसका निर्माण हुआ है।
- यह मिट्टी हल्की एवं अनुपजाऊ होती है।
- इसे क्वार्ट्ज मृदा कहा जाता है।
6. ज्वालामुखी मिट्टी
- नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में यह मिट्टी पायी जाती है।
- आग्नेय चट्टानों के विदीर्ण होने से निर्मित यह मिट्टी हल्की एवं बलुई है तथा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है।
- इस प्रकार की मृदा को ज्वालामुखी मिट्टी कहा जाता है।
7. दोमट मिट्टी
- शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों तथा दून घाटी में सहज ही उपलब्ध इस मिट्टी में हल्का चिकनापन के साथ- साथ चूना, लौह अंश और जैव पदार्थ विद्यमान रहते हैं।
- दोमट मिट्टी दून घाटी में पाई जाती है।
- इसमें चूना तथा लौह अंश की अधिकता होती है।
8. भूरी लाल पीली मिट्टी
- नैनीताल, मंसूरी व चकरौता के निकट चूने एवं बलुवा पत्थर, शेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह मृदा पाई जाती है।
- इसका रंग भूरा, लाल अथवा पीला होता है।
- ऐसा धरातलीय चट्टानों एवं वानस्पतिक अवशेषों के होता है।
- यह मृदा अधिक आद्रता ग्राही और उपजाऊ होती है।
9. लाल मिट्टी
- यह मिट्टी अधिकांशतः पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे पायी जाती है।
- यह मिट्टी असंगठित होती है।
10. वनों की भूरी मिट्टी
- वन की भूरी मिट्टी यह मिट्टी उत्तराखण्ड के अधिकांश वनीय भागों में पायी जाती है।
- इसमें जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी होती है।
11. भस्मी मिट्टी
- यह मिट्टी कम ढालू स्थानों, पर्वत श्रेणियों के अंचलों तथा उप-उष्ण देशीय एवं समशीतोष्ण सम्भगों में पायी जाती है।
12. उच्चतम पर्वतीय छिछली मिट्टी
- यह मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है।
- अत्यधिक शुष्कता तथा वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व होती है।
- इसकी परत पतली होती है।
13. उच्च मैदानी मिट्टी
- यह मिट्टी सामान्यतः 4000 km से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है।
- शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय तथा हिमानी अपरदन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियो में प्रायः नमी की कमी पायी जाती है।
- यह हल्की क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थों के उच्च मात्रा से युक्त होती है।
- चट्टानी टुकड़ों तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण इस मिट्टी के गठन एवं संरचना में विभिन्नता आ जाती है।
- इन्हें एल्पाइन चारागाह (पाश्चर्स) मृदा भी कहते है।
| Read Also : |
|
|---|---|
| Uttarakhand Study Material in Hindi Language (हिंदी भाषा में) | Click Here |
| Uttarakhand Study Material in English Language |
Click Here |
| Uttarakhand Study Material One Liner in Hindi Language |
Click Here |
| Uttarakhand UKPSC Previous Year Exam Paper | Click Here |
| Uttarakhand UKSSSC Previous Year Exam Paper | Click Here |