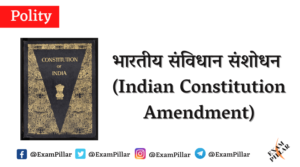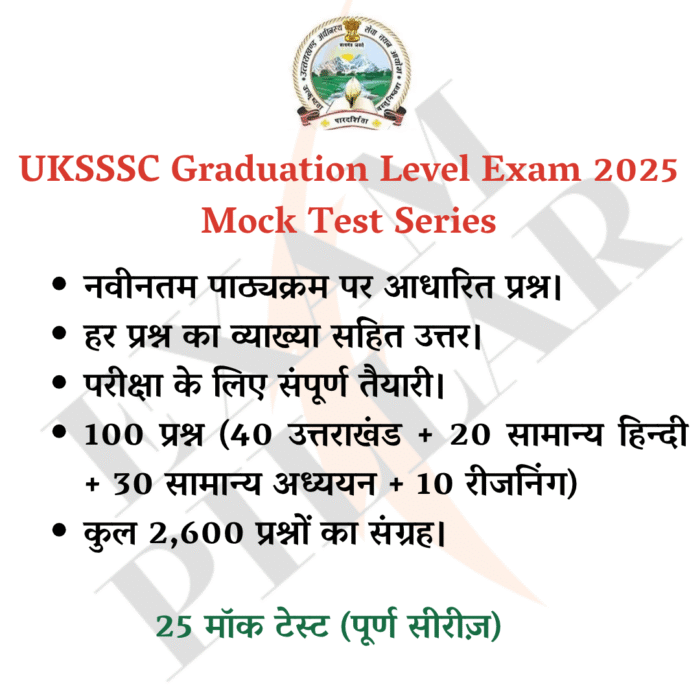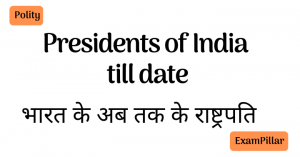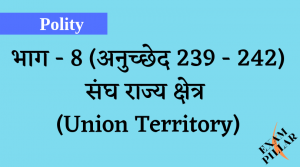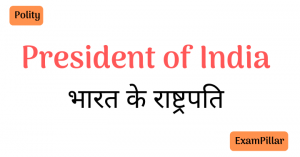संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केवल दिल्ली में ही उच्च न्यायालय है।
वर्तमान समय में पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है। मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा राज्यों तथा दमन, दीव, एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पाण्डिचेरी तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है।
गठन
प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया। जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे (अनुच्छेद 216) साथ ही अनुच्छेद 224 में यह भी प्रावधान है कि नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायाधीश भी दो वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। सभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है।
नियुक्ति
संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। 1993 के उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निश्चित कर दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो सकती।
1999 में उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना अनिवार्य है, किंतु स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीशों से परामर्श को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों, जिससे स्थानांतरण किया गया है। और जिसको स्थानांतरण किया जाना है, उनके मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना भी अनिवार्य होगा।
योग्यता
अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य तभी माना जायेगा, जब वह –
- भारत का नागरिक हो और उसकी 62 वर्ष की आयु पूरी न हुई हो,
- भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर आसीन रहा हो तथा।
- किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 228 के अनुसार, उच्च न्यायाधीश किसी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी अन्य या उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है (अनुच्छेद 233)।
कार्यकाल
अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित तरीकों से पद रिक्त हो सकता है –
- वह स्वयं त्यागपत्र दे ।
- संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर दिया जाये।
- यदि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दे या उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दे।
यहां यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
वेतन तथा भत्ते
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गयी है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन कानून 2018 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रु. प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रु. प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार के भत्ते तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन भी। दी जाती है। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उनके कार्यकाल में उनमें कमी नहीं की जा सकती।
स्थानांतरण
अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकता है।
शपथ ग्रहण
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने के पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी अधिकारी के सम्मुख संविधान के प्रति निष्ठावान रहने तथा अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की शपथ लेनी पड़ती है।
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्ति तथा कार्य
संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां वही होंगी, जो संविधान के प्रारंभ होने के पहले थीं।
आरंभिक या मूल अधिकार क्षेत्र
निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालयों को आरंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।
- संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी अभियोग सीधा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय को न सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर, बल्कि अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
- तलाक, वसीयत, न्यायालय का अपमान, कम्पनी कानून आदि से संबंधित मामले भी उच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
अपीलीय अधिकार क्षेत्र
उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है।
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार
उच्चतम न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गये किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जो संविधान के किसी अनुच्छेद के विरुद्ध हो। उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
अन्तरण संबंधी अधिकार
यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाये कि किसी निम्न न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे में किसी कानून की धारणा का प्रश्न जुड़ा है, तो वह उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है अथवा संबंधित कानून की व्याख्या कर निम्न न्यायालय को मुकदमा वापस भेज सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को अन्तरित कर सकता है।
अभिलेख न्यायालय
संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है।
अधीक्षण क्षेत्राधिकार
प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति है। इस शक्ति के प्रयोग से वह ऐसे न्यायालयों/ अधिकरणों
(i) से विवरण मांग सकता है,
(ii) की कार्यवाही के संबंध में नियम बना सकता है, तथा
(iii) शुल्कों को नियत कर सकता है।
| Read More : |
|---|