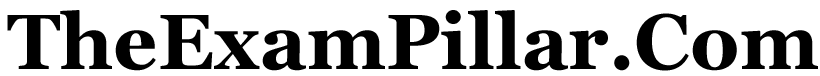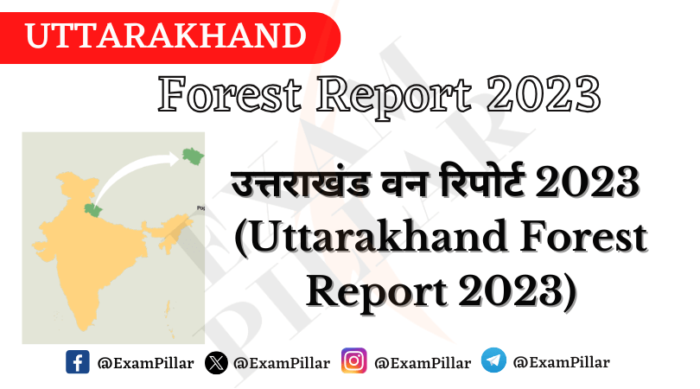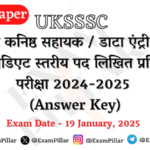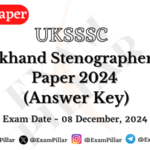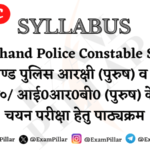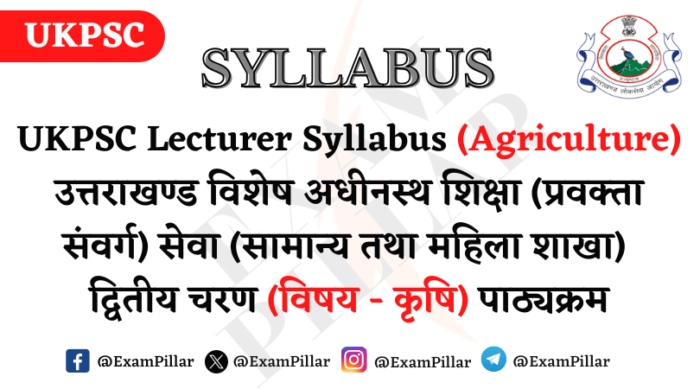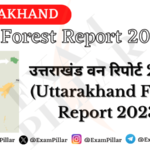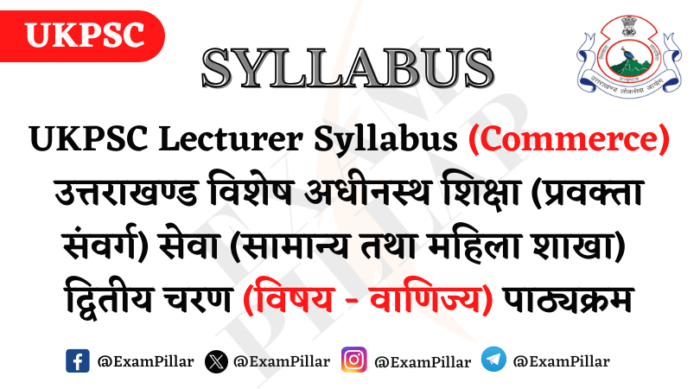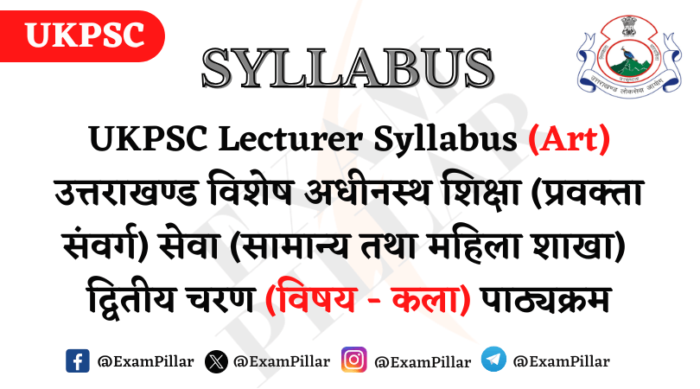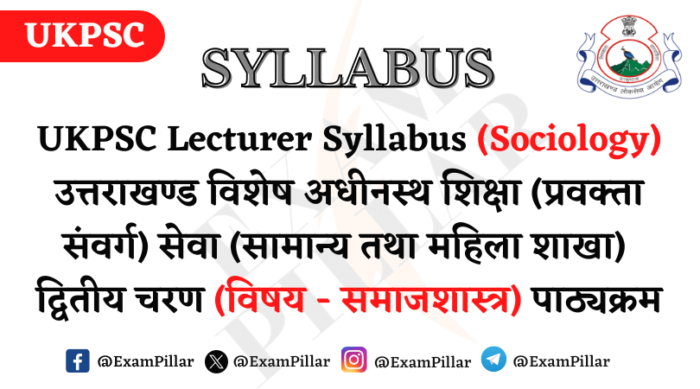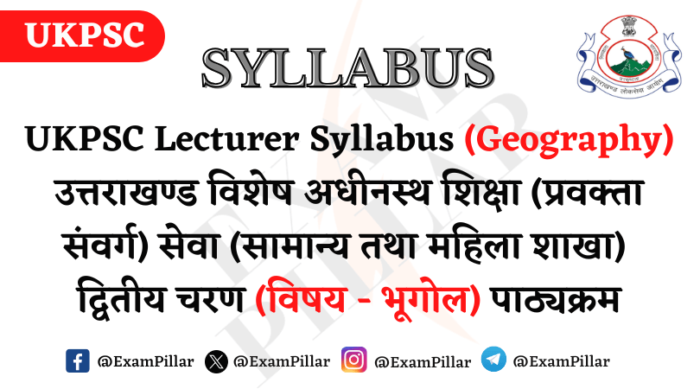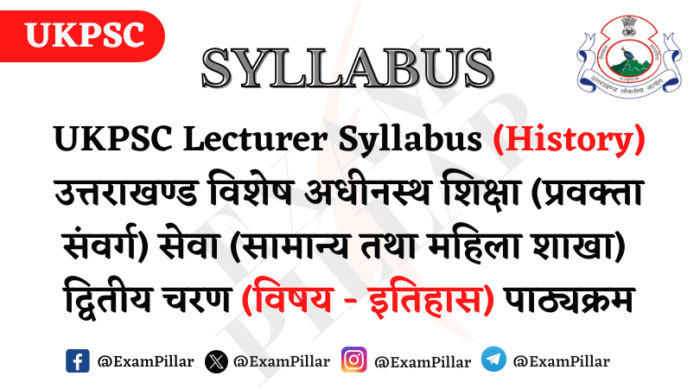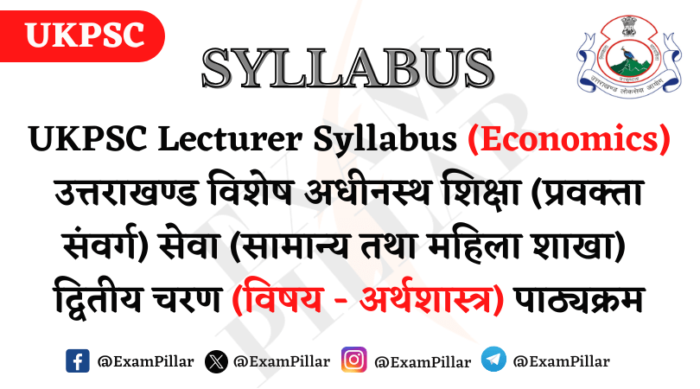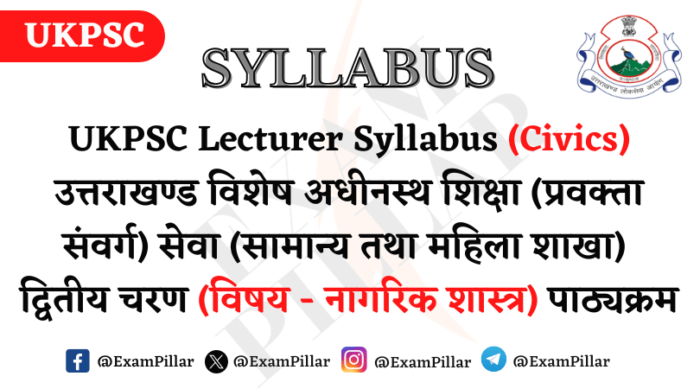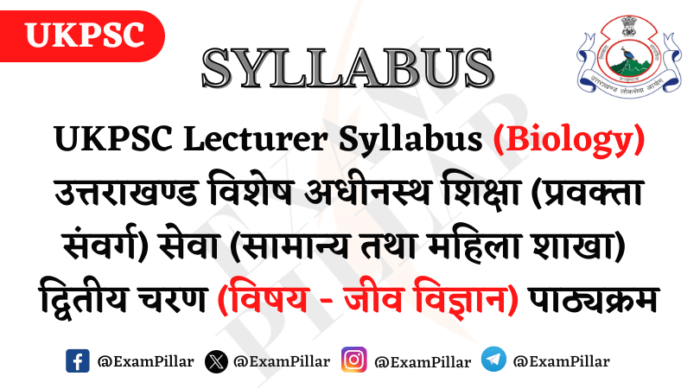उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023
(Uttarakhand Forest Report 2023)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसम्बर 2024 को रिपोर्ट जारी की। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था वर्ष 2023 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report – ISFR) का यह 18वाँ प्रकाशन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से ‘भारतीय वन सर्वेक्षण’ द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
वनों की तीन श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें शामिल हैं–
- अत्यधिक सघन वन (Very Dense Forest) (70% से अधिक चंदवा घनत्व),
- मध्यम सघन वन (Moderately Dense Forest) (40 – 70%) और
- खुले वन (Open Forest) (10 – 40%)।
- स्क्रबस (Scrub) (चंदवा घनत्व 10% से कम) का भी सर्वेक्षण किया गया लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।
भारत में वन आवरण
| श्रेणी | क्षेत्रफल (Km2) | भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत |
| वन आवरण (Forest Cover) | 7,15,342.61 | 21.76% |
| वृक्ष आवरण (Tree Cover) | 1,12,014.34 | 3.41% |
| कुल वन आवरण (Total Forest and Tree Cover ) | 8,27,356.95 | 25.17% |
| झाड़ी (Scrub) | 43,622.64 | 1.33% |
| गैर वन (Non Forest) | 24,16,489.29 | 73.50% |
| कुल भौगोलिक क्षेत्र | 32,87,468.88 | 100% |
उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 (Uttarakhand Forest Report 2023)
17वीं वन रिपोर्ट (2021) की तुलना में उत्तराखंड के कुल वनों में 22.98 वर्ग किमी. की कमी आयी हैं। जिसमे से सात जनपदों में वनों के क्षेत्रफलों में कमी दर्ज की गई हैं।
उत्तराखंड का वन आवरण
| श्रेणी | क्षेत्रफल (Km2) | प्रतिशत |
| अत्यधिक सघन वन (VDF) | 5,266.58 | 9.85% |
| मध्यम सघन वन (MDF) | 12,517.63 | 23.40% |
| खुले वन (OF) | 6,519.62 | 12.19% |
| Total | 24,303.83 | 45.44% |
| स्क्रबस (Scrub) | 412.88 | 0.77% |
उत्तराखंड के जिलेवार वन क्षेत्र
| जनपद | क्षेत्रफल | VDF | MDF | OF | Total | प्रतिशत | Scrub | परिवर्तन 2021 के तुलना में |
| अल्मोड़ा | 3,144.05 | 222.24 | 817.89 | 682.83 | 1,722.96 | 54.80% | 5.82 | 4.09 |
| बागेश्वर | 2,241.00 | 222.24 | 741.21 | 354.43 | 1,263.37 | 56.38% | 1.43 | -2.36 |
| चमोली | 8,030.21 | 442.65 | 1,522.23 | 676.42 | 2,641.30 | 32.89% | 3.78 | -9.36 |
| चम्पावत | 1,765.78 | 382.01 | 571.36 | 266.02 | 1,219.39 | 69.06% | 9.06 | -3.28 |
| देहरादून | 3,088.00 | 680.99 | 588.99 | 370.32 | 1,640.30 | 53.12% | 80.47 | 4.67 |
| पौड़ी गढ़वाल | 5,328.55 | 588.44 | 1,847.84 | 924.27 | 3,360.55 | 63.07% | 99.06 | 0.58 |
| हरिद्वार | 2,360.20 | 76.86 | 274.35 | 213.55 | 564.76 | 23.93% | 11.25 | -2.47 |
| नैनीताल | 4,251.35 | 780.03 | 1,583.17 | 503.35 | 2,866.55 | 67.43% | 15.88 | 0.77 |
| पिथोरागढ़ | 7,090.05 | 518.02 | 978.53 | 640.78 | 2,137.33 | 30.15% | 44.89 | 0.68 |
| रुद्रप्रयाग | 1,984.14 | 272.76 | 582.17 | 291.68 | 1,146.61 | 57.79% | 9.23 | -3.23 |
| टिहरी गढ़वाल | 3,642.17 | 305.87 | 1,149.08 | 767.73 | 2,222.68 | 61.03% | 103.25 | 8.87 |
| ऊधम सिंह नगर | 2,542.25 | 157.69 | 216.42 | 120.06 | 494.17 | 19.44% | 4.53 | -11.29 |
| उत्तरकाशी | 8,015.81 | 671.29 | 1,644.39 | 708.18 | 3,023.86 | 37.72% | 24.23 | -10.65 |
| Grand Total | 53,483.36 | 5,266.58 | 12,517.63 | 6,519.62 | 24,305.13 | 45.44% | 412.88 | -22.98 |
- उत्तराखंड के 6 सबसे ज्याद वन आवरण वाले जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से – पौड़ी गढ़वाल (3,360.55 वर्ग किमी.), उत्तरकाशी (3,023.86 वर्ग किमी.), नैनीताल (2,866.55 वर्ग किमी.), चमोली (2,641.3 वर्ग किमी.), टिहरी गढ़वाल (2,222.68 वर्ग किमी.) व पिथोरागढ़ (2,137.33 वर्ग किमी.)
- उत्तराखंड के 6 सबसे कम वन आवरण वाले जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से – ऊधम सिंह नगर (494.17 वर्ग किमी.), हरिद्वार (564.76 वर्ग किमी.), रुद्रप्रयाग (1,146.61 वर्ग किमी.), चंपावत (1,219.39 वर्ग किमी.), बागेश्वर (1,263.37 वर्ग किमी.) व देहरादून (1,640.30 वर्ग किमी.)
- उत्तराखंड के 6 सबसे ज्याद वन आवरण वाले जनपद प्रतिशत की दृष्टि से – चंपावत (69.06%), नैनीताल (67.43%), पौड़ी गढ़वाल (63.07%), टिहरी गढ़वाल (61.03%), रुद्रप्रयाग (57.79%) व बागेश्वर (56.38%)
- उत्तराखंड के 6 सबसे कम वन आवरण वाले जनपद प्रतिशत की दृष्टि से – ऊधम सिंह नगर (19.44%), हरिद्वार (23.93%), पिथौरागढ़ (30.15%), चमोली (32.89%), उत्तरकाशी (37.72%) व देहरादून (53.12%)
- उत्तराखंड के 6 सबसे ज्याद वन आवरण में कमी वाले जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से – ऊधम सिंह नगर (-11.29 वर्ग किमी.), उत्तरकाशी (-10.65 वर्ग किमी.), चमोली (-9.36 वर्ग किमी.), चम्पावत (-3.28 वर्ग किमी.), रुद्रप्रयाग (-3.23 वर्ग किमी.) व हरिद्वार (-2.47 वर्ग किमी.)
- उत्तराखंड के 6 सबसे ज्याद वन आवरण में वृद्धि वाले जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से – टिहरी गढ़वाल (8.87 वर्ग किमी.), देहरादून (4.67 वर्ग किमी.), अल्मोड़ा (4.09 वर्ग किमी.), नैनीताल (0.77 वर्ग किमी.), पिथोरागढ़ (0.68 वर्ग किमी.) व पौड़ी गढ़वाल (0.58 वर्ग किमी.)
- उत्तराखंड के 6 सबसे ज्याद क्षेत्रफल वाले जनपद – चमोली (8,030 वर्ग किमी.), उत्तरकाशी (8,016 वर्ग किमी.), पिथौरागढ़ (7,090 वर्ग किमी.), पौड़ी गढ़वाल (5,329 वर्ग किमी.), नैनीताल (4,251 वर्ग किमी.) व टिहरी गढ़वाल (3,642 वर्ग किमी.)
- उत्तराखंड के 6 सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद – चंपावत (1,766 वर्ग किमी.), रुद्रप्रयाग (1,984 वर्ग किमी.), बागेश्वर (2,241 वर्ग किमी.), हरिद्वार (2,360 वर्ग किमी.), ऊधम सिंह नगर (2,542 वर्ग किमी.) व देहरादून (3,088 वर्ग किमी.)
उत्तराखंड का ऊंचाईवार वन आवरण
| ऊंचाई क्षेत्र | भौगोलिक क्षेत्रफल | VDF | MDF | OF | Total | Scrub |
| 0 – 500 | 7,937.03 | 713.24 | 1,501.40 | 613.09 | 2,827.73 | 35.56 |
| 500 – 1000 | 5,703.01 | 1,193.46 | 1,830.75 | 913.20 | 3,937.41 | 106.47 |
| 1000 – 2000 | 17,560.08 | 1,546.53 | 5,084.29 | 3,396.26 | 10,027.08 | 230.03 |
| 2000 – 3000 | 7,248.04 | 1,684.12 | 3,003.48 | 1,050.44 | 5,738.04 | 22.55 |
| 3000 – 4000 | 4,193.08 | 129.22 | 1,094.83 | 536.58 | 5,738.04 | 17.11 |
| > 4000 | 10,842.12 | 0.01 | 2.88 | 10.05 | 12.94 | 1.16 |
| Total | 53,483.36 | 5,266.58 | 12,517.63 | 6,519.62 | 24,303.83 | 412.88 |
विभिन्न ढलान वर्ग उत्तराखंड का वन आवरण
| तापमान | भौगोलिक क्षेत्रफल | VDF | MDF | OF | Total | Scrub |
| 0 – 5 | 9,446.02 | 919.17 | 1,371.22 | 646.14 | 2,936.53 | 44.52 |
| 5 – 10 | 4,069.01 | 505.08 | 948.89 | 353.65 | 1,807.62 | 19.02 |
| 10 – 15 | 5,688.06 | 638.36 | 1,474.60 | 652.83 | 2,765.79 | 38.82 |
| 15 – 20 | 7,028.03 | 759.54 | 1,893.38 | 935.23 | 3,588.15 | 60.58 |
| 20 – 25 | 7,313.11 | 756.44 | 2,014.82 | 1,058.30 | 3,829.56 | 70.73 |
| 25 – 30 | 6,683.05 | 667.25 | 1,849.74 | 1,029.67 | 3,546.66 | 68.32 |
| > 30 | 13,256.08 | 1,020.74 | 2,964.98 | 1,843.80 | 5,829.52 | 110.89 |
| Total | 53,483.36 | 5,266.58 | 12,517.63 | 6,519.62 | 24,303.83 | 412.88 |
जंगल की आग
अग्नि सीजन 2022-23 और 2023-24 के दौरान SNPP-VIIRS सेंसर का उपयोग करके FSI द्वारा पता लगाई गई जंगल की आग की जिलेवार संख्या।
| जनपद | SNPP-VIIRS के दौरान पता लगाना (2022-23) | SNPP-VIIRS के दौरान पता लगाना (2023-24) |
| अल्मोड़ा | 786 | 2,810 |
| बागेश्वर | 321 | 805 |
| चमोली | 330 | 1,331 |
| चम्पावत | 470 | 1,782 |
| देहरादून | 230 | 705 |
| पौड़ी गढ़वाल | 928 | 3,193 |
| हरिद्वार | 99 | 59 |
| नैनीताल | 570 | 3,320 |
| पिथोरागढ़ | 785 | 1,204 |
| रुद्रप्रयाग | 70 | 489 |
| टिहरी गढ़वाल | 310 | 2,589 |
| ऊधम सिंह नगर | 128 | 289 |
| उत्तरकाशी | 324 | 2,457 |
| Grand total | 5,351 | 21,033 |
| Read Also : |
|
|---|---|
| Uttarakhand Study Material in Hindi Language (हिंदी भाषा में) | Click Here |
| Uttarakhand Study Material in English Language |
Click Here |
| Uttarakhand Study Material One Liner in Hindi Language |
Click Here |
| Uttarakhand UKPSC Previous Year Exam Paper | Click Here |
| Uttarakhand UKSSSC Previous Year Exam Paper | Click Here |
| MCQ in English Language | Click Here |