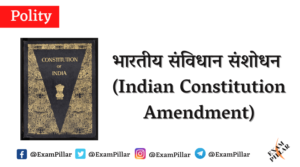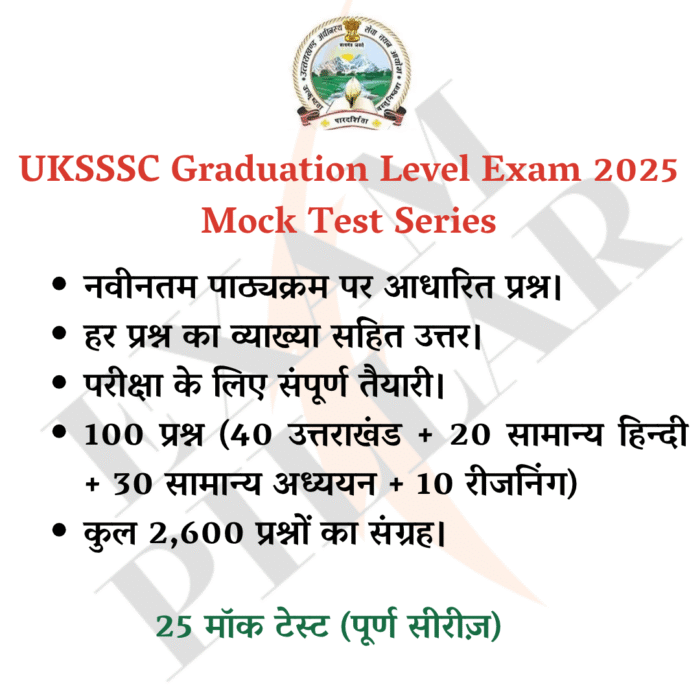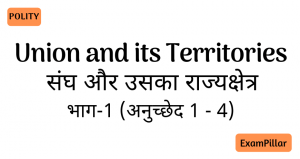पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां (Important Committees for Panchayati Raj)
पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार है –
- बलवंत राय मेहता समिति (1957) – सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- वी.के. राव समिति (1960) – पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्कसंगतता
- एस.डी. मिश्र अध्ययन दल (1961) – पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन
- वी. ईश्वरन अध्ययन दल (1961) – पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन
- जी.आर. राजगोपाल अध्ययन दल (1962) – न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन
- दिवाकर समिति (1963) – ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा
- एम. रामा कृष्णनैया अध्ययन दल (1963) – पंचायती राज संस्थाओं की आय-व्यय गणना का अध्ययन
- के. संथानम समिति (1963) – पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा
- के. संथानम समिति (1965) – पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रुपरेखा सम्बन्धी अध्ययन
- आर.के. खन्ना अध्ययन दल (1965) – पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण।
- जी. रामचंद्रन समिति (1966) – पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन।
- वी. रामानाथन अध्ययन दल (1969) – भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका।
- एम. रामा कृष्णनैया अध्ययन दल (1972) – पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना।
- दया चौबे समिति (1976) – सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा।
- अशोक मेहता समिति (1977) – पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व।
- दांतेवाला समिति (1978) – खण्ड स्तर पर योजना स्वरूप
- हनुमंत राव समिति (1984) – जिला स्तरीय योजना का स्वरूप
- जी.वी.के. राव समिति (1985) – ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम।
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986) – लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तीकरण।
- पी.के. थुगंन समिति (1988) – स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा।
बलवंत राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee)
जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (स्वायतत्ता)’ की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित हैं: –
- तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना-गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिये।
- ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए।
- पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए।
- इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उतरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिएं ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें।
- भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए।
समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी, 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें। किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए।
राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरु द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया।
अशोक मेहता समिति (Ashok Mehta Committee)
दिसंबर 1977 में, जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें कीं । इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार
- त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर, और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होने चाहिए।
- जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।
- ‘न्याय पंचायत’ को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए।
- विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिएं और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए।
समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण, केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी तीन राज्य कर्नाटक, पं० बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए।
जी.वी.के. राव समिति (G. V. K. Rao Committee)
ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलम कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया किया। समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें कीं, जो इस प्रकार थीं:
- जिला स्तरीय निकाय, अर्थात् जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये।
- जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिये।
- पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिये।
जी.वी.के.राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दाँतवाला समिति, 1978 तथा जिला आयोजना पर हनुमंत राव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेन्द्रित आयोजना का कार्य जिला स्तर पर सम्पन्न किया जाना चाहिए।
एल.एम. सिंघवी समिति (L. M. Singhvi Committee)
1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती। राज संस्थाओं का पुनरुद्धार’ पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल.एम. सिंहवी की अध्यक्षता में किया। इसने निम्न सिफारिशें दीं :-
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाये। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज निकास के नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी।
- गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाये।
- ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना।
- गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिये न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये।
थुगन समिति (Thumban Committee)
1988 में, संसद की सलाहकार समिति की एक उप-समिति पी. के. थुगन की अध्यक्षता में राजनीतिक औ प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गयी। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की थी:
- पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं का पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए।
- एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि छह माह होनी चाहिए।
- पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए।
- पंचायती राज के तीन स्वरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए।
- हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता-बिंदु तथा विधियां तय करेगा।
- जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलक्टर होगा।
गाडगिल समिति (Gadgil Committee)
1988 में वी. एन. गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता। इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएँ की थी।
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
- गाँव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए।
- पचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए।
- पंचायत के सभी तीन स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए।
- अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेवारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाएँगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे।
- पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा।
गाडगिल समिति की ये अनुशंसाएँ एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनीं। इस विधेयक का लक्ष्य था-पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना।
| Read More : |
|---|