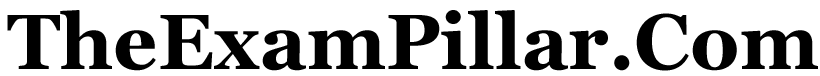संत कवि कबीर (Sant Kavi Kabir)
संत कबीर अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न और महिमा युक्त महामानव थे। कबीर की भक्ति ने भारतीय जनमानस को उस समय अवलम्बन प्रदान किया था जब वह सिद्धों और योगियों की गुहासाधना से आतंकित हो रही थी। कबीर के समय धार्मिक क्षेत्र में अनेक धर्म साधनाएँ प्रचलित थी जो जनता को उकसा रही थी। इस महान सन्त आत्मा ने अपनी प्रेमाभक्ति का ऐसा संबल और दृढ़ अवलम्बन धर्म प्राण जनता को प्रदान किया कि वह राम-रस में भाव-विह्वल हो डूब उठी। कबीर की भक्ति का यह आदर्श नवीन होते हुए भी सर्वथा भारतीय है। उसमें प्रेम, विश्वास और ज्ञान का सम्मिश्रण है। एक ओर तो वह प्रेम और विश्वास की छटा से अलौकिक है तो दूसरी ओर वह चिन्तन के विविध आयाम भी प्रस्तुत करती है। एक ओर कबीर निर्गुण की बात करते हैं तो दूसरी ओर ईश्वर के दर्शन की कामना भी करते हैं। इस रुप में कबीर की भक्ति में रामानन्द का भक्तिवाद, इस्लाम का एकेश्वरवाद, नाथ पंथ का हठयोगवाद और सूफियों की प्रेमनिष्ठा का समन्वय है।
कबीर की भक्ति का आदर्श ऊँचा है। उसमें प्रेम, अगाध विश्वास, श्रद्धा आस्था और निष्ठा है किंतु पूजा अनुहान के लिए अवसर कम हैं। कबीर में भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति जब अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो वह अपने आराध्य की निकटता करती है, ऐसे में भौतिक उपासना गौण हो जाती है। कबीर की सम्पूर्ण भक्ति, प्रेम, विश्वास चित्त की शुद्धता और ज्ञान के आधार पर ही टिकी है।
कबीर का ज्ञान भी अद्भुत है। वह वेदों और शास्त्रों का होते हुए भी इनके प्रतिकूल है। वह आत्मानुभूतियों पर टिका है इसलिए इसमें विराटता है, वह देश, काल और ग्रंथों की परिधि से परे असीम है। वह किसी एक धर्म, सम्प्रदाय और मत-विशेष से जुड़ा न होकर सबका है।
कबीर की सम्पूर्ण रचनाएँ पदों, साखियों, शब्दों और रमैनियों में हैं। उन्होनें दोहे में विभिन्न राग- रागनियों को अपनी रचनाओं में ढाला है। इनमें क्रमबद्धता और सुसम्बद्धता नहीं है, इसका कारण उन्हें छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं था और उन्होनें सचेष्ट होकर इनकी रचना नहीं की थी।
कबीर के कहने का ढंग भी अपने तरीके का अनूठा है। उस पर कबीर के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है कबीर के व्यक्तित्व की अक्खड़ता और निर्भयता जैसे उनकी शैली में समाहित हो गई है।
कबीर का जीवन वृत्त
कबीर का जन्म कब हुआ इस सम्बन्ध में विद्धान एकमत नहीं हैं। ‘कबीर चरित्र बोध’ के अनुसार कबीर का जन्म संवत् 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को हुआ। कबीर पंथियों की मान्यता का आधार यह पद है:
“चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ गये।
जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रगट भये।।
धन गरजे दामिनी दमके, बूंद करखे झर लाग भरे।
मल खिले तहं कबीर भानु प्रगट भये।।”
कबीर की जन्मतिथि के सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध है, वह केवल कबीर पंथियों में प्रचलित ये दोहे ही हैं। ज्योतिषाचार्य और गणिताचार्यों की गणना के अनुरुप भी कबीर की जन्मतिथि संवत् 1455 ही मानी चाहिए अत: यह तिथि अधिक प्रामाणिक है।
कुल और जाति
कबीर पंथियों के विश्वासानुसार कबीर लहरतारा में कमल पत्र पर प्रकाश स्वरूप अवतीर्ण हुए थे। अन्य मत के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राहमणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोकापवाद के भय से नवजात कबीर को काशी में लहरतारा तालाब के निकट फैंक दिया था, जहां नीरु नामक जुलाहे ने उन्हें आश्रय दिया था। इन दोनों मतों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता।
कबीर की रचनाओं के आधार पर यह तथ्य उभर कर आता है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था और उनके पिता का नाम नीरु जुलाहा और माता का नाम नीमा था। कबीर जिस जुलाहा वंश में उत्पन्न हुए थे हो सकता है कि किसी भय अथवा प्रलोभन के चलते उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया हो। आचार्य हजारी प्रसाद विवेदी जी ने अपनी पुस्तक कबीर में लिखा है ‘ ‘कबीरदास की वाणियों में जान पड़ता है कि मुसलमान होने के बाद न तो जुलाहा जाति अपने पूर्ण के संस्कारों से एकदम मुक्त हो सकी थी और न उनकी सामाजिक मर्यादा बहुत ऊँची हो सकी थी। पर कबीर की रचनाओं से यह बात प्रमाणित नहीं होती कि वे मुसलमान थे क्योंकि उन्होंने अपनी वाणियों में स्वयं के न हिंदू और न मुसलमान होने की बात कही है।
कबीर की वाणियों से तो यह सिद्ध होता है कि कबीर नाथपंथ से जुड़ी योगी जाति में उत्पन्न हुए थे जो सचमुच न हिन्दू थी, न मुसलमान। इस जाति के मनुष्यों का व्यवसाय कपडा बुनना था।
कबीर की शिक्षा
दीक्षा कुछ भी नहीं हुई और यदि कुछ हुई भी हो तोइसके विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर कबीर की वाणियों और साखियों से यह ज्ञात होता है कि उनके भीतर ही शान जैसे अन्तर्भूत था।
कबीर का ज्ञान किताबी न होकर अनुभवीय था। उनका हृदय दिव्य प्रकाश से भरा था। वे घुमक्कड़ प्रकृति के थे और अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राएँ भी करते थे। वे हिन्दू साधु और मुस्लिम फकीरों की सत्संगति में रहते थे। इस सत्संग से कबीर को बहुत लाभ हुआ। इसी से उन्हें भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं के शब्दों का ज्ञान हुआ और वे हिन्दू शास्त्रों और मुस्लिम धर्म ग्रन्थों से परिचित हुए।
परिवार
कबीर का विवाह लोई से हुआ था। कुछ लोग कबीर की पत्नी का नाम रामजनियां मानते थे। कबीर के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की भांति ही उनका पुत्र कमाल भी संत और कवि हृदय था। जिसने कबीर की अपूर्ण रचनाओं को पूर्ण किया।
कबीर के हृदय में बाल्यावस्था से ही भक्ति अंकुरित हो उठी थी। कबीर की परिपक्वावस्था के साथ-साथ यह भक्ति भी पुष्ट होती गई। अपने जीवन की सांध्य-बेला में वे गृहस्थ जीवन से भी विरत हो उठे थे।
कबीर के मृत्यु-संवत् के सम्बन्ध में भी मतभेद है। कबीर की मृत्यु के सम्बन्ध में कबीर की मृत्यु के सम्बन्ध में ज्ञात तथ्यों के आधार पर संवत् 1575 में उनका निधन होना माना है। उन्होंने 120 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त की थी।
कबीर पंथियों के अनुसार कबीर की मृत्यु पर हिन्दुओं और मुसलमानों में विग्रह उत्पन्न हो गया था। हिन्दू अपनी परम्परा के अनुसार कबीर के शव को जलाना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना चाहते थे। ऐसे में कबीर के शव के स्थान पर कमल के फूल प्राप्त हुए जिसे उन दोनों ने आपस में बांटकर अपनी- अपनी विधि का निर्वाह किया।
कबीर की रचनाएँ
कबीर कवि और काव्यप्रणेता नहीं थे। वे पहले भक्त और सुधारक हैं, कवि बाद में। यही कारण है कि उन्होंने अपनी धुन में ही आत्माभिव्यक्ति कर पदों की रचना की और अपनी सत्संग मंडली में उनको सुनाया करते थे। कबीर के पदों से और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोग इनके शिष्य बने। इन्हीं शिष्यों ने कबीर के निधन के उपरान्त कबीर के पदों, साखियों और रमैनियों को संकलित किया, जो ‘बीजक’ के नाम से प्रसिद्ध हुई। ‘बीजक’ के अतिरिक्त भी कबीर के नाम से कई संग्रहित ग्रंथ प्राप्त होते हैं, इनमें कुछ ग्रंथ हस्तलिखित भी हैं। इनमें से कई रचनाएं प्रक्षिप्त हैं जो बाद में उनके शिष्यों द्वारा जोड़ दी गई है कबीर द्वारा रचित मानी जाने वाली रमैनियों का उल्लेख कई छोटे-बड़े ग्रंथों में हुआ है।
‘बीजक’ में रमैनी, साखी और सबद का समावेश है। इनकी रचना गायन की दृष्टि से की गई है अतः इनमें विषयवस्तु की आवृत्ति भी दिखाई देती है। ऐसे में साखियों में कबीर की आध्यात्मिक मान्यता के दर्शन होते हैं।
कबीर के साहित्य की पृष्ठभूमि
कबीर एक ऐसे युग में उत्पन्न हुए थे जब भारतीय समाज निराशा और दीनता के समुद्र में डूब रहा था। कबीर ने निराशा के घने अंधकार में डूबे भारतीय समाज को अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दिया।
कबीर का युग दुर्व्यवस्था और अस्तव्यस्तता का युग था। मुसलमानों के आक्रमण भारत पर निरन्तर होते रहते थे जिससे भारत की आंतरिक शक्ति क्षीण हो रही थी। विदेशी मुसलमानों ने दिल्ली पर आधिपत्य पर लिया था। हिन्दू जनता पूरी तरह से निराश हो रही थी। अपनी राष्ट्रीयता के प्रति उनमें विश्वास पूर्ण रूप से समाप्त हो चला था। ये हिन्दु राजा मुसलमान शासकों को प्रसन्न करने के लिए अपने ही भाईयों का गला काटने पर तुले थे। भारतीय समाज की राजनैतिक शक्ति अब बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। सामाजिक स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही थी। वेदों के एकेश्वरवाद के स्थान पर अनेक प्रकार के धर्म और सम्प्रदाय प्रचलित थे। धर्म, ईश्वर और धर्म ग्रंथ केवल उच्चवर्ग तक मित रह गया था। धर्म के नाम पर पापाचारों का बोलबाला था।
चारों ओर बाह्याडम्बरों, पंडों, पुजारियों और धर्म गुरुओं का प्रभुत्व था। छूआछूत की भावना बड़ी तीव्रता के साथ फैल रही थी। वर्ण व्यवस्था अब जड़ और रूढ़ होकर रह गई थी। प्रेम और मानवीयता की भावनाएं धीरे-धीरे तिरोहित होती जा रही थी। चारों तरफ सामाजिक और राजनीतिक विश्रृंखलता छाई थी। काशी नगरी जो धर्म का केन्द्र थी, में कुछ लोग धर्म के नाम पर विलासिता कर रहे थे तो करोड़ों लोग दुःख और अभावों से भरे चीत्कार कर रहे थे। समाज में दलित वर्ग के लिए कोई संवेदना शेष नहीं रह गई थी। वे समाज की उपेक्षा और घृणा के पात्र रह गए थे। ऐसे में यह वर्ग भी मानवता रहित, ऐसे समाज का परित्याग कर रहा था। वर्ण-व्यवस्था की संकीर्णता और छापा-तिलक, माला और धर्म ग्रन्थों की रक्षा में संलग्र समाज के प्रति उनके मन में कोई भावना शेष नहीं थी।
कबीर ने अपने युग के दलितों की इन भावनाओं की तड़पन को देखा और उनका हृदय उनकी पीड़ा से आर्द्र हो उठा। उन्होंने उस समाज के प्रति अपने विद्रोह को बुलन्द किया, जो मनुष्यता को कुचल रहा था। उन्होंने विरोध किया और संघर्ष किया। तत्कालीन समाज के हीन, दलित और उपेक्षित वर्ग की ओर से समाज को ललकारा और फटकार। कबीर के पदों और वाणियों में आदि से अंत तक यही स्वर सुनाई देते हैं।
कबीर की भाषा
कबीर के काव्य में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी के साथ ही खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। अतः व्याकरण की दृष्टि से भी इस भाषा में मिश्रित प्रवृति अथवा शैली दिखाई देती है।
डॉ. श्याम सुन्दर दास ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखा है – “कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। कबीर में केवल शब्द ही नहीं क्रियापद कारण चिनादि भी कई भाषाओं में मिलते है। कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे इसी से बाहरी प्रभावों के बहुत शिकार हुए। भाषा और व्याकरण की स्थिरता उनमें नहीं मिली। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में अक्खड़पन है और साहित्यिक कोमलता या प्रसाद का सर्वथा अभाव है। कहीं-कहीं उनकी भाषा गॅवारू लगती है।”
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर की भाषा पर लिखा है – “कबीर साहब के ग्रंथों का आदर कविता की दृष्टि से नहीं, विचार दृष्टि से है। कहीं-कहीं उनकी भाषा में गॅवारुपन आ जाता है।”
आचार्य हजारी प्रसाद दविवेदी ने कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए व्यक्त किया कि – “भाषा पर कबीर का जबर्दस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है, बन गया है तो सीधे-सादे नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कह सके।”
संदर्भ –
- कबीर – आचार्य हजारी प्रसाद विवेदी
- कबीर साहित्य की परख – आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
- कबीर एक अनुशीलन – डॉ. रामकुमार वर्मा
- कबीर का रहस्यवाद – डॉ. रामकुमार वर्मा
- कबीर साहित्य चिन्तन – आचार्य परशुराम चतुर्वेदी