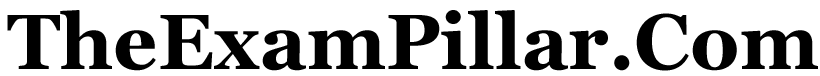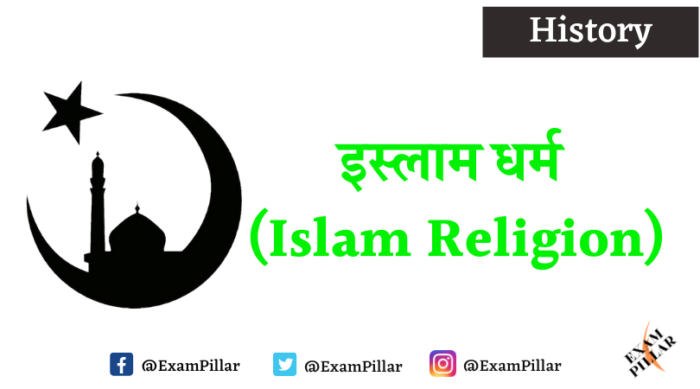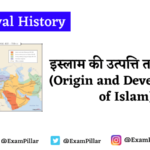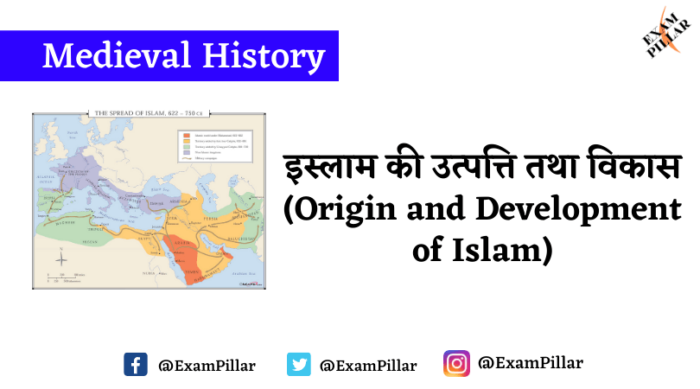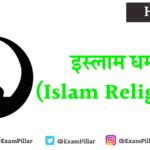इस्लाम धर्म
(Islam Religion)
‘इस्लाम (Islam)’ का शाब्दिक अर्थ ‘आत्म समर्पण’ है। यह एक ईश्वर परक धर्म है। इस धर्म में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। इस्लाम धर्म (Islam Religion) के संस्थापक पैगम्बर मुहम्मद साहब (Prophet Muhammad) माने जाते हैं। इनका जन्म 570 ई. में अरब के मक्का नामक स्थान पर हुआ था। हजरत मुहम्मद जब 40 वर्ष के हुए तो उन्हें ‘सत्य के दिव्य दर्शन’ हुए और वे पैगम्बर बन गये। पैगम्बर बनने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। दिव्य दर्शनों के बाद मुहम्मद साहब को पूर्ण विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और वे ही ईश्वर के पैगम्बर हैं। इस्लाम की मान्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सर्वशक्तिमान अल्लाह में और अल्लाह के पैगम्बर के शब्दों में आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा के सामने मनुष्य की कोई शक्ति नहीं है, अतः मनुष्य का ईश्वर की इच्छा के आगे झुकना श्रेयस्कर है। इस धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं –
- अल्लाह या खुदा एक है तथा सभी मनुष्य उसके बंदे हैं।
- अल्लाह इल्हाम अर्थात् सच्चा ज्ञान अपने पैगम्बरों को देता है।
- इस्लाम की दृष्टि में सभी समान हैं।
- इस्लाम के अनुयायियों को हर रोज पांच बार नमाज पढ़नी चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए।
- निर्धनों और भिक्षुओं की मदद करनी चाहिए।
- इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखना चाहिए।
- ब्याज लेना, जुआ खेलना, शराब पीना और सूअर का माँस खाना अनिवार्य रूप से निषेध माना जाता है।
सूफी आंदोलन (Sufi Movement)
एक अवधारणा है कि सूफी शब्द अरबी भाषा के ‘सफा’ से बना, जो कि पवित्रता का समानार्थी है, इस प्रकार जीवन में आध्यात्मिकता एवं पवित्रता का अनुपालन करने वाला सूफी कहे जाने लगे। सूफी आंदोलन भी भक्ति आंदोलन की तरह अपने प्रभाव में मध्यकाल मे आया। इस्लाम धर्म में चलने वाले रहस्यवादी दर्शन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। सूफी संतों ने सादगीपूर्ण जीवन बिताते हुए आमजनों के बीच नैतिकता का विकास किया एवं इस्लाम को और उदार बनाने की कोशिश की।
सूफी धर्म की अवस्थाएँ (States of Sufi Religion)
- तौबा (पश्चाताप)
- वार (विरक्ति)
- जहद (पवित्रता)
- फक्र (निर्धनता)
- सब्र (धैर्य)
- शुक्र (कृतज्ञता)
- खौफ (भय)
- रजा (आशा)
- तबक्कुल (संतोष)
- रिजा (ईश्वर की इच्छा के प्रति अधीनता)
भारत में सूफियों का आगमन (Arrival of Sufis in India)
भारत में सूफी मत का आगमन 11वीं और 12वीं शताब्दी से माना जाता है। किंतु, 13वीं-14वीं शताब्दी आते-आते यह कश्मीर, बिहार, बंगाल तथा दक्षिण तक फैल चुका था, जबकि पहले सूफियों का मुख्य केंद्र मुल्तान व पंजाब था।
अबूल फजल ने आइने अकबरी में सूफियों के 14 सिलसिलाओं का वर्णन किया है। जो मुख्यतः दो प्रकार के दर्शनिक धाराओं में बंटे हुए हैं –
वहदत-उल-वजूद
सूफी दर्शन की यह धारा अधिक लोकप्रिय थी। कश्मीर में प्रचलित एवं भारत के अन्य हिस्सों में (दिल्ली सहित) नक्शबंदी को छोड़कर अधिकांश सिलसिलाएँ इससे ही जुड़े हुए थे। ये खुदा और व्यक्ति बीच के अस्तित्व एकता की बात करता है। इस धारा के एक सन्त मंसूर ने ‘अनल हक’ (मैं ही खुदा हूँ) का दावा किया था। ये लोग व्यक्ति के अंदर छिपे हुए खुदा की प्राप्ति के लिए प्रेममार्ग पर चलने के लिए बल देते थे। इन संतों ने प्रेम के विकास के लिए कई आचरण एवं नियम बनाए, इसके साथ ही ये शमां, और फना (पार्थिव अस्तित्व को भूल जाना) पर भी बल देते थे।
वहदत-उल-सुहूद
इस धारा के विचारक ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं और व्यक्ति को खुदा का बन्दा। इन्होंने खुदा और व्यक्ति के बीच की एकता को असंभव बताया ये शमां (संगीत) का विरोध करते थे।
मुख्य सूफी सम्प्रदाय एवं उनसे जुड़े प्रमुख संत
चिश्ती संप्रदाय
इस संप्रदाय के संत सादगी और निर्धनता में आस्था रखते थे। इसे चिश्तिया संप्रदाय भी कहते हैं, इसके प्रथम संत शेख मुईनुद्दीन चिश्ती थे, जो ख्वाजासाब के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म पूर्वी ईरान के सिजिस्तान नामक प्रांत में हुआ। ये प्रारंभ में लाहौर में रहे फिर अजमेर में स्थाई रूप से बस गए। ख्वाजा साहब का निधन 1236 ई. में हुआ। अजमेर इनकी दरगाह है। चिश्ती संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण संत हमीदुद्दीन नागौरी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज-ए-शकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरूद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती आदि थे।
सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय
यह भी सूफियों का महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसके प्रणेता शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय वहाउद्दीन जकारिया को दिया जाता है, जो कि 13वीं सदी के प्रभावशाली सूफी संत थे। सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय के अन्य प्रभावशाली संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी, सद्रद्दीन आरिफ रूकनुद्दीन को बहुत सम्मानित स्थान मिला। इस संप्रदाय में उनकी स्थिति वैसी ही थी, जैसी चिश्तिया संप्रदाय में निजामुद्दीन औलिया की थी।
कादिरी संप्रदाय
इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दिया जाता है, जिन्होंने 12वीं सदी में इस संप्रदाय को स्थापित किया। भारत में कादिरी संप्रदाय के पहले संत शाह नियामत उल्ला और नासिरूद्दीन महमूद जिलानी थे। इस संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण संत थे-मियाँ मीर और मुल्ला शाह बदख्शीं। मुलग सम्राट शाहजहाँ का बड़ा बेटा कादरी सूफी संप्रदाय से प्रभावित होकर इसका अनुयायी बन गया था।
नक्शबंदी संप्रदाय
इस संप्रदाय के प्रणेता ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी (1317-89 ई.) को माना जाता है। भारत में इस संप्रदाय के प्रचारक बकी बिल्लाह (1563-1603 ई.) थे, जो बहाउद्दीन के सातवें उत्तराधिकारी थे। इस संप्रदाय ने इस्लाम में नए परिवर्तनों का विरोध किया तथा पैगम्बर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने पर बल दिया। नक्शबंदी संप्रदाय के महत्वपूर्ण संतों के नाम इस प्रकार हैं – शेख अहमद सरहिन्दी, शाह वली उल्लाह एवं ख्वाजा मीर दर्द।
कलन्दरिया संप्रदाय
इस संप्रदाय का प्रचार-प्रसार सैय्यद शाह नज्मुद्दीन कलंदर ने किया। वह सैय्यद खिज्र रूमी के शिष्य थे। इस संप्रदाय के अनय महत्वपूर्ण संत थे-कुतुबुद्दीन कलंदर और शरीफुद्दीन अली कलन्दर।
शत्तारिया संप्रदाय
सूफी संप्रदाय की इस शाखा को ईरान एवं मध्य एशिया में ‘इश्किया’ तथा तुर्की में ‘विस्तामिया’ नाम से जाना जाता है। शत्तारिया संप्रदाय में ‘शत्तर’ से आशय गति से है। इस संप्रदाय की यह विशिष्टता है कि इसमें साधक को कम समय में ‘फना’ और ‘बका’ की अवस्था मिल जाती है। भारत में शत्तारिया संप्रदाय के प्रवर्तक शेख अब्दुला शत्तार को माना जाता है। इस संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण संत शाह गौस और शाह बहाउद्दीन थे।
|
प्रमुख सूफी कवि और रचनाएँ |
|
| कवि | रचना |
| मुल्ला दाऊद | चंदायन |
| उस्मान | चित्रवली |
| शेखनबी | ज्ञानद्वीप |
| कुतुबन | मृगावती |
| नूर मुहम्मद | अनुराग बांसुरी, इंद्रावती |
| कासिम शाह | हंस जवाहिर |
| जायसी | पदमावत, अखराट, आखिरी कलाम, कन्हावत |
| मंझन | मधुमालती |
| Read Also : |
|---|