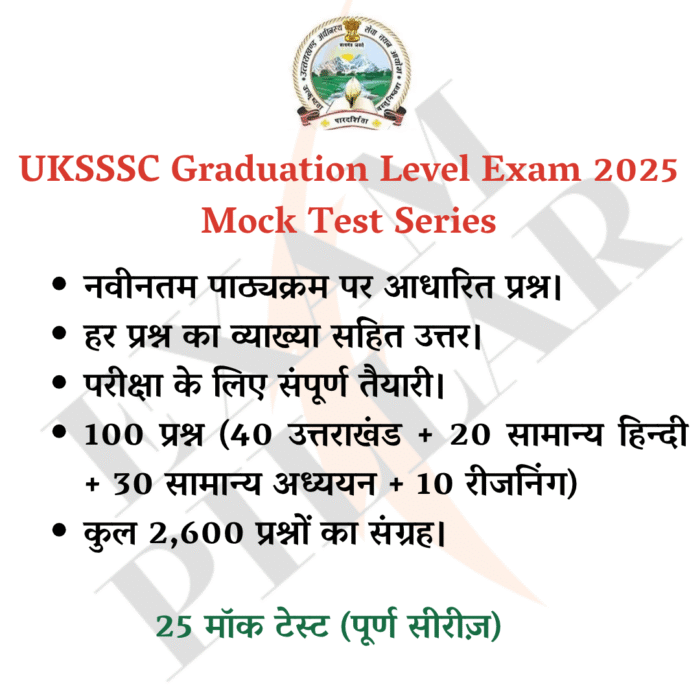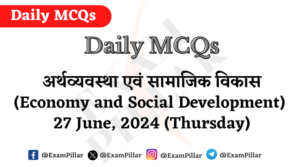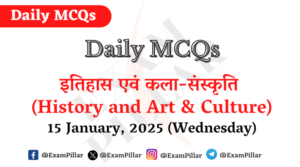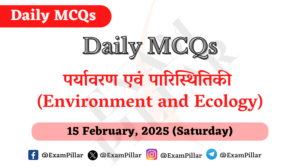Daily MCQs : संविधान एवं राजव्यवस्था (Constitution and Polity)
10 February, 2025 (Monday)
1. मौलिक अधिकारों बनाम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. गोलकनाथ केस, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है।
2. संसद किसी भी मौलिक अधिकार के प्रशासन में सुधार के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में पूरी तरह से संशोधन कर सकती है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
व्याख्या – मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ‘भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित किया गया है। दोनों के बीच यह सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। संसद निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान या नष्ट नहीं करता है। हालाँकि, संसद अपनी सनक और सनक के आधार पर निदेशक सिद्धांतों में संशोधन नहीं कर सकती है और भारतीय संविधान की ‘कल्याणकारी राज्य’ की साख को प्रभावित नहीं कर सकती है क्योंकि यह मूल संरचना का एक हिस्सा है। अतः दोनों कथन सही नहीं हैं।Show Answer/Hide
2. राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा।
2. यदि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेजा गया कोई विधेयक बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित हो जाता है, तो राज्यपाल पर विधेयक पर अपनी सहमति देने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
व्याख्या – अनुच्छेद 200 में प्रावधान है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल घोषित करेगा- अतः कथन 2 सही नहीं है।Show Answer/Hide
(a) कि वह विधेयक पर सहमति देता है; या
(b) कि वह उस पर सहमति रोक देता है; या
(c) कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है; या
(d) राज्यपाल, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए एक संदेश के साथ विधेयक (धन विधेयक के अलावा) को वापस कर सकता है। लेकिन, यदि विधेयक विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित हो जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति नहीं रोकेंगे; या
(e) यदि राज्यपाल की राय में, विधेयक, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को इतना कम कर देगा कि इसकी संवैधानिक स्थिति को खतरे में डाल देगा, वह इस पर सहमति नहीं देगा, लेकिन इसे विचार के लिए आरक्षित कर देगा। अध्यक्ष।
3. भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तरीके से राज्य के अंगों का कार्यात्मक पृथक्करण निर्धारित करता है?
1. राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।
2. संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
3. संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि जब किसी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही चल रही हो।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
व्याख्या – भारत का संविधान राज्य के अंगों को निम्नलिखित तरीके से कार्यात्मक पृथक्करण प्रदान करता है :- अनुच्छेद 50: राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 122 और 212: संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह प्रक्रियात्मक अनियमितता के आरोप पर न्यायिक हस्तक्षेप से विधायिकाओं की पृथक्करण और प्रतिरक्षा सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती है। क्रमशः अनुच्छेद 53 और 154 में प्रावधान है कि संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित होगी और उन्हें नागरिक और आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त होगी। अनुच्छेद 361: राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। अतः सभी कथन सही हैं।Show Answer/Hide
4. यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधीन है या नहीं, तो किसका निर्णय अंतिम होगा और क्यों?
(a) मुख्यमंत्री क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है
(b) राज्य विधानमंडल क्योंकि यह राज्य के भीतर सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है
(c) राज्य का राज्यपाल क्योंकि संविधान उसे यह अधिकार प्रदान करता है
(d) भारत के राष्ट्रपति जो राज्यपाल को सलाह देते हैं
व्याख्या – यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक के अंतर्गत आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा, और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी काम की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उसके विवेक में. साथ ही, संविधान कहता है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। अतः कथन (c) सही है।Show Answer/Hide
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग III में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की पुष्टि करता है।
2. अनुच्छेद 32 के तहत गारंटीकृत अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे निलंबित किया जा सकता है।
3. मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना स्वयं एक मौलिक अधिकार है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?
(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं
व्याख्या – यह संविधान में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों में से एक है जिसका प्रत्येक नागरिक हकदार है। अनुच्छेद 32 ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार’ से संबंधित है, या संविधान के भाग III में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। 1975 के आपातकाल के दौरान, एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित रहेगा। 44वें संशोधन में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 32 के तहत, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने के आदेश जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 के अपवाद के साथ (की सुरक्षा से संबंधित है) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामले में कुछ अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा)। दीवानी या आपराधिक मामलों में, पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध पहला उपाय ट्रायल कोर्ट है, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। जब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात आती है, तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 226, हालांकि, अनुच्छेद 32 की तरह मौलिक अधिकार नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है।Show Answer/Hide