
Daily MCQs – अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास – 14 November 2024 (Thuesday)
Daily MCQs : अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास (Economy and Social Development) 14 November, 2024 (Thursday) 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित

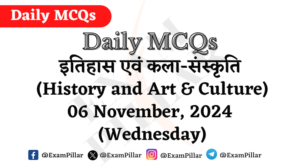
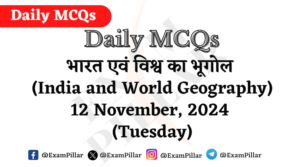
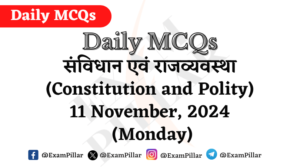
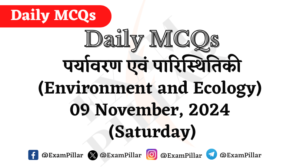
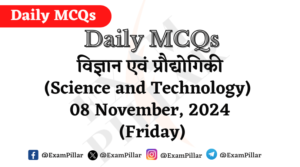
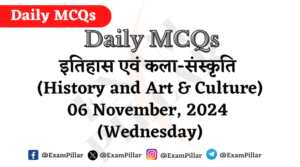

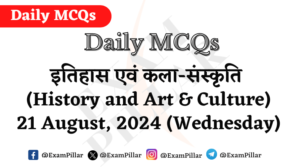
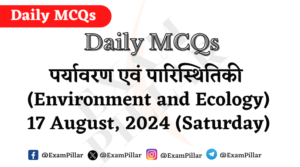
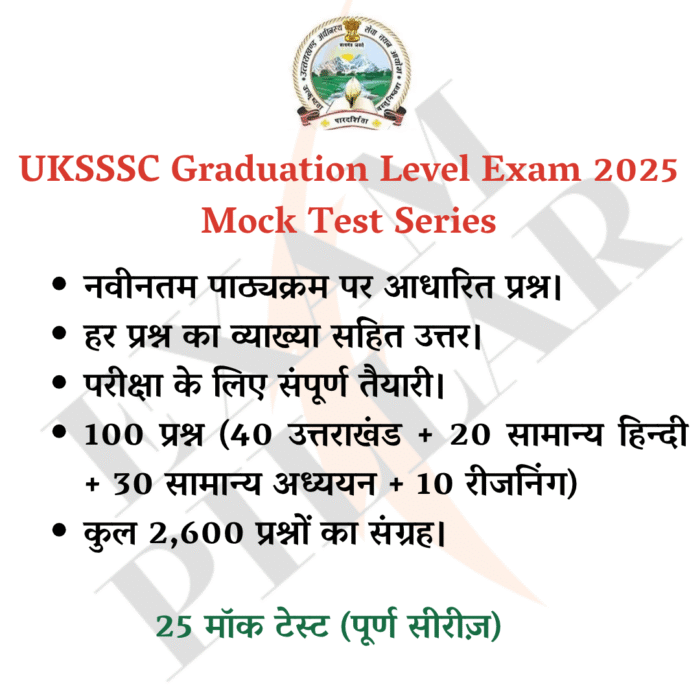

SOCIAL PAGE